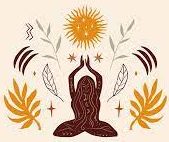‘भारतीयों ने कभी आक्रमण नहीं किया’ एक मिथक है। गुप्त, चोल, ललितादित्य मुक्तापिड़ा विजेता थे
राष्ट्रकूटों ने हिमालय, तमिलनाडु पर छापा मारा; चोलस बंगाल, इंडोनेशिया; कश्मीरी पंजाब, अफगानिस्तान और शिनजियांग। मध्यकालीन भारतीयों में विजय के लिए एक बड़ी भूख थी।

सूर्य मंदिर, मार्तंड, जम्मू और कश्मीर।
Oमध्यकालीन भारत के बारे में सबसे व्यापक मिथकों में से एक यह है कि हमारे पूर्वज दुनिया के बाकी हिस्सों के प्रति “शांतिपूर्ण” थे और “भारत की सीमाओं” के बाहर किसी भी सैन्य गतिविधियों में उदासीन थे। इसकी तुलना, स्पष्ट रूप से, अरबों और तुर्कों के विस्तार से की जाती है, जो माना जाता है कि अन्य शांतिपूर्ण, समृद्ध भूमि को जीतने और नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे। जबकि कुछ लोग स्वीकार करेंगे कि भारतीय शासकों के युद्ध किसी भी अन्य के युद्धों की तरह क्रूर थे, ऐसा लगता है कि जब तक युद्ध “हमारे अपने” के साथ थे, वे किसी भी तरह से अन्य संस्कृतियों की तुलना में गुणात्मक रूप से अलग और “बेहतर” थे।
ब्रिटिश औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा हम पर थोपी गई अधिकांश व्याख्याओं की तरह, यहां अनपैक करने के लिए बहुत कुछ है। पहली अंतर्निहित धारणा यह है कि मध्ययुगीन भारत – अपने चौंका देने वाले आकार और विविधता के बावजूद – “हम और वे” की स्पष्ट भावना के साथ कुछ प्रकार की सांस्कृतिक एकता थी, जो किसी भी तरह से आधुनिक राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के साथ काफी आसानी से मेल खाती है। दूसरा, एक धारणा है कि मध्ययुगीन दुनिया में युद्ध ठीक उसी कारण से लड़ा गया था जो पूरे समय हर दूसरे संदर्भ में लड़ा गया था। यह एक शानदार उबाऊ विचार है, जो अपने लिए विस्तार और विजय की औपनिवेशिक मानसिकता से आता है। जैसा कि हम सबूतों का पता लगाते हैं, हम देखेंगे कि मध्ययुगीन भारत में भूगोल, विस्तार और युद्ध के विचार पूरी तरह से आधुनिक रूढ़ियों को धता बताते हैं।
“कोर” से विस्तार: गंगा साम्राज्य
हमारे आधुनिक राष्ट्र-राज्य की सीमाओं के बाहर “भारतीय” सैन्य गतिविधियों के सबूत मिलना एक साधारण बात है। श्रीलंका के एक मध्ययुगीन क्रॉनिकल कुलावम्सा में बताया गया है कि कैसे चोल राजवंश द्वारा द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। दक्षिण भारतीय शिलालेख खंड II में, चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम ने विवरण दिया है कि कैसे उनके सैनिकों ने वर्तमान मलेशिया और इंडोनेशिया में श्रीविजय संघ को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मैं यहां कुछ और महत्वाकांक्षी करना चाहता हूं – यह स्थापित करने के लिए कि चोल कोई अपवाद नहीं थे और जब भी यह संभव था, भारतीय राजनीति “विदेशों” को जीतने की कोशिश कर सकती थी और करती थी।
शुरू करने के लिए, आइए एक गंगा साम्राज्य को देखें – जो 4 वीं शताब्दी ईस्वी के गुप्तों का था – जिसने मध्ययुगीन काल में हमारे द्वारा देखे जाने वाले कई सांस्कृतिक और राजनीतिक पैटर्न को गति दी। गुप्त काल के ग्रंथों से ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि उपमहाद्वीप के बाहर के लोग विजय के कम योग्य थे। कालिदास के रघुवमसम में, पौराणिक राजा रघु को उन सभी लोगों को हराने के रूप में वर्णित किया गया है जो अपने पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर में रहते थे। कैंटो 4, वचन 60 में उन्हें “पारसिकाओं या फारसियों की विजय पर आगे बढ़ने” का श्रेय दिया गया है, जिसके दौरान “उन्होंने अर्धचंद्राकार तीरों से उनके दाढ़ी वाले सिर काट दिए” (पद 63)। इसके तुरंत बाद, हमें बताया गया कि उसने सिंधु नदी पार कर ली, और यह कि “हुना [हून] महिलाओं के गालों पर फ्लश ने रघु के कार्यों को अपने स्वामी पर प्रदर्शित किया” (वचन 68); कि “कम्बोज [अफगान] अपने महान पौरुष का विरोध करने में असमर्थ थे”; और यह कि उन्होंने विभिन्न हिमालयी जनजातियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पहुंचे और अंत में अपनी राजधानी अयोध्या लौट आए, इस प्रकार चार दिशाओं की अपनी विजय पूरी की।
हम देख सकते हैं कि युद्ध के लिए प्रेरणा एनेक्सेशन नहीं है। अपने किसी भी अभियान में रघु ने गवर्नर या वाइसरायल्टी की स्थापना नहीं की। इसके बजाय, वह श्रद्धांजलि और प्रतीकवाद से प्रेरित है: सभी चार कार्डिनल दिशाओं में अपनी भारी सैन्य शक्ति (और पौरुष) का प्रदर्शन करके, इस प्रकार दिग्विजय या “दिशाओं की विजय” का प्रदर्शन करके – वह खुद को एक सार्वभौमिक संप्रभु, एक चक्रवर्ती के रूप में स्थापित करता है। भले ही हम रघुवमसम के अधिकांश दावों को साहित्यिक अतिशयोक्ति के रूप में खारिज कर सकते हैं, फिर भी यह हमें कुछ महत्वपूर्ण बताता है: कि मध्ययुगीन भारत में युद्ध के लिए प्रेरणा जटिल थी, प्रतीकात्मकता के साथ-साथ धन से प्रेरित थी; और यह कि उपमहाद्वीप “समाप्त” है, इसका कोई स्पष्ट भौगोलिक या सांस्कृतिक अर्थ नहीं था।
“सीमा” से विस्तार: कश्मीर का मामला
अगर हम यह स्थापित करना चाहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप से परे विस्तार करने में रुचि नहीं रखते थे, तो हमें उन राजनीतिओं के उदाहरण खोजने की आवश्यकता है, जिन्होंने – यहां तक कि जब विकल्प दिया गया था – जानबूझकर इन काल्पनिक आधुनिक सीमाओं से परे युद्ध नहीं छेड़ने का फैसला किया।
ऐसा उदाहरण मध्ययुगीन कश्मीर से आ सकता है। 8 वीं शताब्दी ईस्वी में, गंगा के मैदानों में अराजकता की स्थिति के साथ, कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापिड़ा ने खुद को एक ऐसी स्थिति में पाया जहां वह इस उपजाऊ क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से छापा मार सकता था। और फिर भी 12 वीं शताब्दी के पाठ, कल्हण की राजतरंगिणी में, हमें एक बार फिर बताया गया है कि उन्होंने कन्नौज, बंगाल (पूर्व), दक्कन (दक्षिण), और द्वारका (पश्चिम) पर छापा मारा। इन सभी का विवरण धुंधला है, लेकिन उत्तर में उनकी विजय – वर्तमान शिनजियांग, तिब्बत और अफगानिस्तान में – शानदार हैं। पुस्तक IV, श्लोक 165-168 में, हमें बताया गया है कि “कम्बोजों के अस्तबल घोड़ों से खाली हो गए थे … तुहखरा [टोचरियन]… पर्वत श्रृंखलाओं में भाग गए … भौटा [तिब्बतियों] द्वारा महसूस की गई चिंता उनके चेहरे पर नहीं देखी जा सकती थी, जो सफेद हैं …” चीनी सूत्र भी अंतिम पंक्ति की पुष्टि करते हैं: ललितादित्य को तांग राजवंश के दरबार में एक दूतावास भेजने के लिए जाना जाता है, जिसमें तिब्बतियों के खिलाफ गठबंधन की पेशकश की गई थी।
कल्हण दो दिलचस्प सांस्कृतिक अवलोकन भी प्रदान करता है (पद 178-180): “इस शक्तिशाली राजा ने विजय प्राप्त शासकों को उनकी हार का संकेत देने के लिए, विभिन्न विशिष्ट चिह्नों को अपनाने के लिए मजबूर किया, जिन्हें वे और उनके लोग आज भी विनम्रता से पहनते हैं। स्पष्ट रूप से, यह उनकी आज्ञा से है, अपने बंधन के निशान को प्रदर्शित करने के लिए, कि तुरुश्का [तुर्क] अपनी बाहों को अपनी पीठ पर रखते हैं और अपना आधा सिर मुंडवाते हैं। दक्षिणात्यों [दक्कनियों] की कमर पर राजा ने पूंछ रखी जो जमीन को साफ करती है, यह चिह्नित करने के लिए कि वे जानवरों की तरह थे। यहां कल्हणा केवल अपने समय की मौजूदा प्रथाओं का वर्णन कर रहे हैं और उन्हें अपने नायक ललितादित्य से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी यह आश्चर्यजनक है कि उनके लिए, दक्कनी तुर्कों की तरह विदेशी हैं, और उन सभी का उल्लेख यह स्थापित करने के लिए किया गया है कि ललितादित्य ने सभी चार दिशाओं में विजय प्राप्त की, इस प्रकार एक सार्वभौमिक सम्राट बन गए।
इसमें शामिल दूरियां कोई भी हों, और सांस्कृतिक अंतर या समानता के बावजूद, सबूत हमें यह दिखाते हैं कि मध्ययुगीन भारतीय राजनीति हमेशा एक प्रतीकात्मक “सार्वभौमिक” शासन स्थापित करने के लिए कार्डिनल निर्देशों का पालन करते हुए अपनी दुनिया के किनारों पर सैन्य विस्तार में रुचि रखती थी।
ऐसा होता है कि उनके ब्रह्मांड हमसे अलग थे: क्योंकि उनकी कल्पनाएं एक राष्ट्र-राज्य द्वारा बाधित क्यों होंगी जो अगले हजार वर्षों तक अस्तित्व में नहीं होगा? दक्कन की राजनीति जैसे राष्ट्रकूटों ने हिमालय, ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु की ओर हमला किया; चोल जैसी तमिल राजनीति ने बंगाल, कर्नाटक, श्रीलंका और इंडोनेशिया की ओर हमला किया; कश्मीरी राजनीति ने पंजाब, अफगानिस्तान और शिनजियांग की ओर हमला किया। एक बार जब हम समझ जाते हैं कि वे सभी अपने स्वयं के चार-दिशात्मक राजनीतिक ब्रह्मांड बनाने की कोशिश कर रहे थे, युद्ध के माध्यम से विस्तार कर रहे थे और अपनी राजधानियों में केंद्रित थे, तो हम “उपमहाद्वीप को एकजुट करने” की ऐतिहासिक धारणाओं की तुलना में कुछ अधिक भव्य देखते हैं: एक चुनौतीपूर्ण दुनिया जहां मध्ययुगीन भारतीय किसी भी अन्य राजनीति की तुलना में विजय की भूख में अलग नहीं थे।